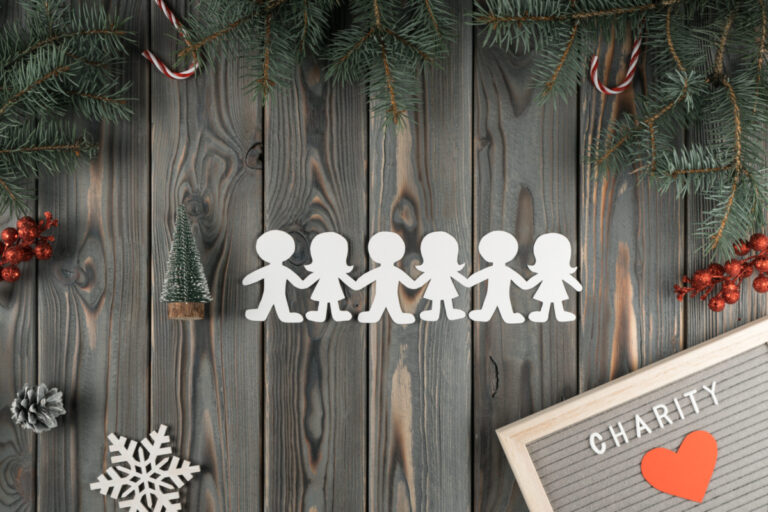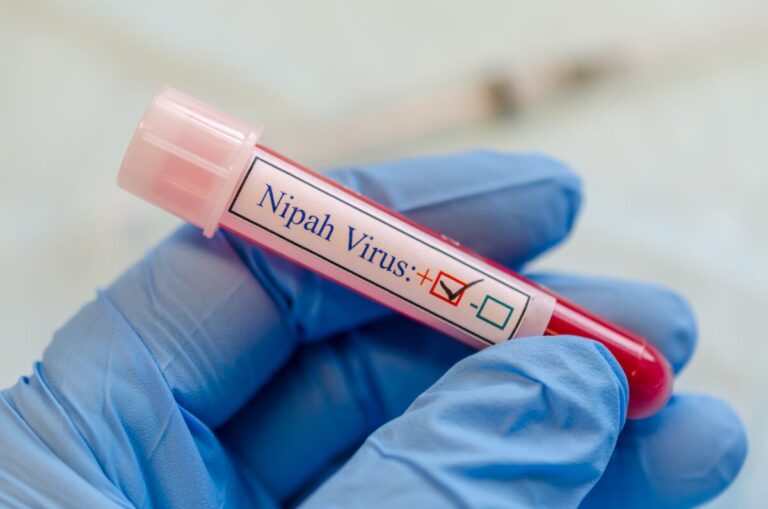Table of Contents
- पार्किंसन रोग कैसे होता है? / पार्किंसन रोग क्या है?
- पार्किंसंस रोग के प्रकार / पार्किसन बीमारी
- पार्किंसन डिजीज के लक्षण / पार्किसन रोग के लक्षण
- पार्किंसंस रोग के कारण / पार्किंसंस रोग कैसे होता है?
- पार्किंसन डिजीज के चरण
- पार्किंसंस रोग का निदान
- पार्किंसंस रोग की रोकथाम
- पार्किंसंस रोग का उपचार / पार्किंसन डिजीज का इलाज
- क्या पार्किंसन डिजीज जीवन के लिए ख़तरा है?
- पार्किंसन डिजीज के लिए सर्वाइवल रेट्स
- पार्किंसन डिजीज के इलाज में लगनेवाला समय
- पार्किंसंस रोग के साथ कैसे लड़ें?
- निष्कर्ष
- पार्किंसन रोग कैसे होता है? / पार्किंसन रोग क्या है?
- पार्किंसंस रोग के प्रकार / पार्किसन बीमारी
- पार्किंसन डिजीज के लक्षण / पार्किसन बीमारी के लक्षण
- पार्किंसंस रोग के कारण / पार्किंसंस रोग कैसे होता है?
- पार्किंसन डिजीज के चरण
- पार्किंसंस रोग का निदान / पार्किसन बीमारी का निदान
- पार्किंसंस रोग की रोकथाम / पार्किसन बीमारी की रोकथाम
- पार्किंसंस रोग का उपचार / पार्किंसन डिजीज का इलाज
- क्या पार्किंसन डिजीज जीवन के लिए ख़तरा है?
- पार्किंसन डिजीज के लिए सर्वाइवल रेट्स
- पार्किंसन डिजीज के इलाज में लगनेवाला समय
- पार्किंसंस रोग के साथ कैसे लड़ें?
- निष्कर्ष
पार्किंसन रोग कैसे होता है? / पार्किंसन रोग क्या है?
पार्किंसंस रोग (पीडी), एक न्यूरोडीजेनेरेटिव डिसऑर्डर है। यह डिसऑर्डर या विकार मुख्य रूप से मस्तिष्क के एक विशिष्ट क्षेत्र में डोपामाइन-उत्पादक, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है, जिसे सबस्टैंटिया नाइग्रा भी कहा जाता है। इस स्थिति का ज़िक्र पहली बार, ब्रिटिश सर्जन डॉ. जेम्स पार्किंसन ने अपनी किताब(जो 1817 में पब्लिश्ड हुई थी) “An Essay on the Shaking Palsy” में की थी। पार्किंसन डिसऑर्डर से लोग तब परिचित होने लगे, जब यह धीरे-धीरे लोगों को अपना शिकार बनाने लगी। वर्तमान में, दुनिया भर में सात से दस मिलियन लोग पार्किंसन डिजीज से प्रभावित होते हैं।
भारत में, आँकड़ों के अनुसार दस लाख लोग पार्किंसंस से पीड़ित हैं। पार्किंसंस से प्रभावित लोग ख़ुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि वह कमज़ोर क्यों महसूस कर रहे हैं, दरअसल यह पार्किंसंस रोग के लक्षण होते हैं।
पार्किंसन डिजीज अक्सर 60 साल या उससे अधिक की उम्र वाले लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन इसके लगभग 4% मामले 50 साल से कम उम्र वाले लोगों में भी मिल सकते हैं। 50 साल से कम उम्र वाले लोगों को होनेवाले पार्किंसन डिसऑर्डर को, यंग-ऑनसेट पार्किंसंस डिजीज कहा जाता है। पार्किंसन डिजीज मानव मस्तिष्क के भीतर होती है, और गति को प्रभावित करने के साथ सोचने की क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है।
पार्किसन बीमारी या पार्किंसन डिजीज, मस्तिष्क के एक हिस्से, सबस्टैंटिया नाइग्रा में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की कमी या मृत्यु के कारण होती है। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स मानव मस्तिष्क को मूवमेंट, स्मृति, अटेंशन, मूड और कई अन्य कार्यों को करने में मदद करता है।
पार्किसन बीमारी जैसे-जैसे बढ़ती है, डोपामाइन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करता है, की कमी होने लगती है, और पार्किंसन डिजीज के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर खुशी, संतुष्टि, प्रेरणा को महसूस कराने के लिए सिग्नल भेजता है। पार्किंसन डिजीज या पार्किंसन रोग क्या है, यह सवाल अब तक सबके सामने एक पहेली बनी हुई है, लेकिन इसके विकसित होने के कारण आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक माने जा सकते हैं।
पार्किंसंस रोग के प्रकार / पार्किसन बीमारी
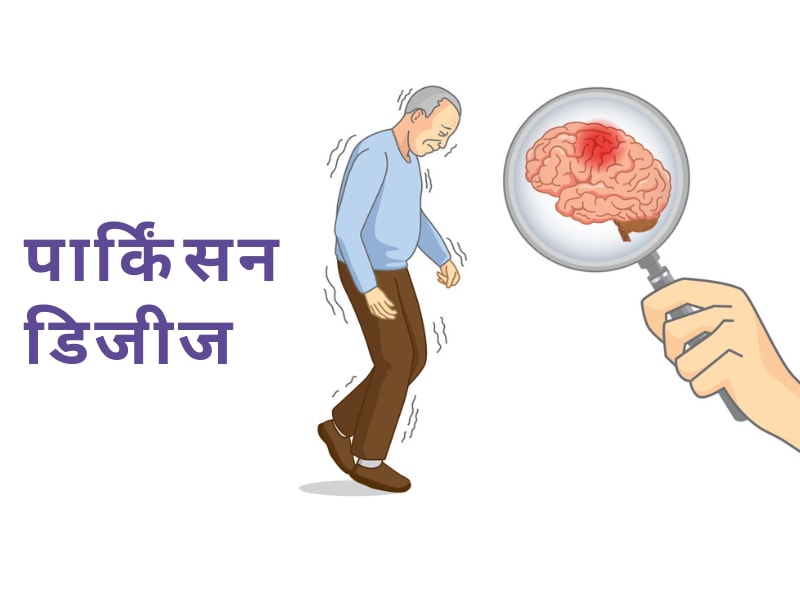
पार्किंसन डिजीज के कई प्रकार हैं और शुरूआती अवस्था में पार्किंसन डिजीज के लक्षण बहुत ही सूक्ष्म होने के कारण पकड़ में ही नहीं आते हैं। पार्किंसन डिजीज के कुछ प्रकार निम्न हैं:
1. इडियोपैथिक / स्पेसिफ़िक पार्किंसंस डिजीज: इडियोपैथिक या स्पेसिफ़िक पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसंस के सबसे आम प्रकारों में से एक है और इसके अधिकतर मामले पाए जा सकते हैं। इडियोपैथिक या स्पेसिफ़िक पार्किंसंस डिजीज के लक्षण शुरुआत में सूक्ष्म होते हैं, और यह अक्सर शरीर के एक तरफ़ ही विकसित होता है, धीरे-धीरे यह शरीर के दूसरे तरफ़ फैलता है। जैसे-जैसे यह रोग प्रगति करता है, इसके लक्षण भी समय के साथ बढ़ते हैं। पार्किंसन रोग कैसे होता है, इसका अभी तक कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाया है। इसका कारण अज्ञात होने की वजह से इसे “इडियोपैथिक” शब्द दिया गया है।
2. यंग-ऑनसेट पार्किंसंस डिजीज(YOPD): यंग-ऑनसेट पार्किंसंस डिजीज, यंग लोगों में पाया जाता है। आमतौर पर यह डिजीज 50 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को होता है। यंग-ऑनसेट पार्किंसन डिजीज अन्य PD डिजीज की तुलना में कम आम है, और इसके मामले सभी PD डिजीज के मामलों में से लगभग 2% -10% पाए जा सकते है। YOPD धीरे-धीरे प्रगति करनेवाली बीमारी है, जिससे व्यक्ति का प्रोडक्टिव येअर(60-70 वर्ष की उम्र) भी प्रभावित होता है। YOPD के लक्षण भी अक्सर इडियोपैथिक के लक्षण जैसे ही होते हैं, लेकिन इसके लक्षण धीरे-धीरे प्रगति करते हैं। वाईओपीडी के लक्षण, शुरुआत में डिस्टोनिया रोग(न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर) के रूप में दिख सकते हैं।
3. पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम / एटिपिकल पार्किंसनिज़्म: पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम या एटिपिकल पार्किंसनिज़्म, न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों का एक समूह है जो पार्किंसंस रोग के कुछ लक्षणों के साथ प्रकट होता है, लेकिन इसकी और भी विशेषताएँ होती हैं और यह अधिक तेज़ी से प्रगति करता है। पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम में, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी (एमएसए), प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी (पीएसपी), कॉर्टिकोबैसल डीजनरेशन (सीबीडी), और लेवी बॉडीज के साथ डिमेंशिया (डीएलबी) शामिल हैं। मानक पीडी दवाइयों का असर इन स्थितियों पर कुछ ख़ास नहीं होता है, और रोगी की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है।
पार्किंसन डिजीज के लक्षण / पार्किसन रोग के लक्षण
पार्किंसन डिजीज के लक्षणों को, मोटर और नॉन-मोटर श्रेणियों(कैटेगरी) में बाँटा गया है। पार्किंसन डिजीज के लक्षण, शरीर के एक ओर से शुरू होते हैं और धीरे-धीरे दूसरी ओर को प्रभावित करते हैं। शुरुआत में पार्किंसन डिजीज के लक्षण सूक्ष्म होते हैं। मोटर लक्षण को अधिकांश, पार्किंसन डिजीज के लक्षण माने जाते हैं और वह लक्षण इस प्रकार हैं:
1. कँपकँपी: कँपकँपी, पार्किंसन डिजीज के लक्षण में से एक लक्षण है और यह शुरूआती लक्षण है। यह लक्षण हाथ या उँगलियों में प्रकट हो सकता है। पार्किंसन डिजीज का एक लक्षण, आराम करते समय हाथ में होनेवाली कँपकँपी है। पार्किंसन के हर केस में यह आवश्यक नहीं है कि कँपकँपी जैसे लक्षण प्रकट हों।
2. ब्रैडीकिनेसिया (गति का धीमा होना): ब्रैडीकिनेसिया भी पार्किंसन डिजीज के लक्षण में से एक है। पार्किंसन डिजीज के बढ़ने के साथ, रोगी के कार्य करने की गति भी धीमी हो जाती है, और उसे सरल कार्यों को करने में भी कठिनाई होने लगती है।
3. मांसपेशियों का कठोर होना: पार्किंसन डिजीज के लक्षण में, मांसपेशियों का कठोर होना शामिल है। इस बीमारी में शरीर के किसी भी हिस्से में मांसपेशियाँ कठोर हो सकती हैं। मांसपेशियों की कठोरता, गति की सीमा को सीमित करने और मांसपेशियों में दर्द का कारण बन सकती है।
4. संतुलन और समन्वय संबंधित समस्याएँ: पार्किंसन डिजीज के बढ़ने से संतुलन और समन्वय संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। संतुलन और समन्वय संबंधित समस्याएँ भी, पार्किंसन डिजीज के लक्षण में शामिल हैं।
पार्किंसंस के नॉन-मोटर लक्षण चलने-फिरने जैसी गतिविधियों से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन मोटर लक्षणों की तुलना में दैनिक जीवन में अधिक तनाव और निराशा का कारण बन सकते हैं। पार्किंसंस के नॉन-मोटर, मोटर लक्षणों से पहले प्रकट हो सकते हैं, और कभी-कभी अधिक दिखाई देने वाले शारीरिक लक्षणों से वर्षों पहले प्रकट होते हैं, इसलिए इन्हें प्री-मोटर लक्षण भी कहा जाता है। सूँघने की क्षमता का कम होना, डिप्रेशन और कॉन्स्टिपेशन जैसे लक्षण वास्तविक निदान से वर्षों पहले प्रकट हो सकते हैं। पीडी के गैर-मोटर लक्षणों में शामिल हैं:
1. मूड डिसऑर्डर: पार्किंसन डिजीज के लक्षण में मूड में बदलाव होना शामिल है। पार्किंसन रोग में व्यक्ति डिप्रेशन या एंग्जायटी का अनुभव कर सकता है।
2. नींद नहीं आना: पीडी में नींद संबंधित समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। नींद में कमी होना पार्किंसन डिजीज के लक्षण में से एक लक्षण है।
3. संज्ञानात्मक परिवर्तन: पार्किंसन डिजीज में, संज्ञानात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे- स्मृति, ध्यान, कार्यकारी कार्य (योजना, समस्या-समाधान), और नेत्र संबंधी कौशल, पार्किंसन डिजीज के लक्षण में शामिल हैं।
4. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम (एएनएस) की शिथिलता: पार्किंसंस के कुछ गैर-मोटर लक्षण, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, शरीर द्वारा ऑटोमेटिकली किए जाने वाले कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे रक्तचाप, हृदय गति, पसीना आदि। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में परिवर्तन होने पर, कब्ज, मूत्र, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन (खड़े होने पर रक्तचाप में गिरावट), और यौन रोग संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
5. सूँघने की क्षमता कम होना: पीडी के कई केसेस में, मोटर लक्षणों की शुरुआत से वर्षों पहले सूँघने की क्षमता कम होने लगती है। सूँघने की क्षमता कम हो जाना, पार्किंसन डिजीज के लक्षण में शामिल हैं।
पार्किंसंस रोग के कारण / पार्किंसंस रोग कैसे होता है?
पार्किंसंस रोग का सटीक कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है, लेकिन इसके विकास के कारणों में आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक शामिल हो सकते हैं।
1. आनुवंशिक कारक: पार्किंसंस रोग के लगभग 10% -15% मामलों में जेनेटिक फैक्टर्स जैसे कारक, कारण पाए जा सकता हैं। पार्किंसंस रोग के विकास के कारणों में एसएनसीए, एलआरआरके2, पीआरकेएन, पिंक1 और डीजे-1 जैसे विशिष्ट जीनों में उत्परिवर्तन शामिल हैं।
2. पर्यावरणीय कारक: पार्किंसंस रोग के कारणों में, कुछ पर्यावरणीय कारक जैसे, ग्रामीण जीवन, कुऍं के पानी का संपर्क, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स के जोखिम शामिल हो सकते हैं। यह जोखिम कारक आनुवंशिक रूप से अतिसंवेदनशील व्यक्तियों में भी पीडी के विकास का कारण बन सकते हैं।
पार्किंसन डिजीज के चरण
पार्किंसंस रोग के चरणों को पाँच चरणों में विभाजित किया गया है। चरणों की जानकारी से पीडी रोग की प्रगति का पता चल सकता है, और आगे उपचार के लिए प्लानिंग भी जा सकती है। पार्किंसंस रोग के चरण निम्न हैं:
1. चरण I: पार्किंसंस के पहले चरण में, हल्के लक्षण प्रकट हो सकते हैं, जैसे शरीर का केवल एक तरफ़ या एक ओर प्रभावित हो सकता है। पहले चरण के लक्षणों में, एक हाथ में हल्का सा कंपन, मुद्रा में बदलाव और चेहरे के भाव में बदलाव शामिल हैं।
2. चरण II: दूसरे चरण में, शरीर का दोनों तरफ़ का हिस्सा प्रभावित होना शुरूहो जाता है, लेकिन संतुलन में कोई हानि नहीं होती है। इस चरण के लक्षणों में शरीर के दोनों तरफ़ कठोरता, कँपकँपी और चेहरे की अभिव्यक्ति में बदलाव शामिल हो सकते हैं।
3. चरण III: इस चरण में गति धीमी होने के साथ, संतुलन की हानि का अनुभव भी किया जा सकता है। कपड़े पहनने और खाने जैसे कार्यों में दिक्कत हो सकती है।
4. चरण IV: पीडी के चौथे चरण में चलने और खड़े होने की क्षमता कम हो सकती है। दैनिक जीवन में कार्यों को करने में कठिनाई का अनुभव किया जा सकता है।
5. चरण V: यह चरण पार्किंसंस का अंतिम चरण और सबसे उन्नत चरण होता है। इस चरण में, सभी दैनिक गतिविधियों को करने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त मतिभ्रम और भ्रम जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस चरण में रोगी की विशेष चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है।
पार्किंसंस रोग का निदान
पार्किंसंस रोग के निदान के लिए सबसे पहले डॉक्टर, रोगी के चिकित्सा इतिहास और रोग के लक्षणों के बारे में पूछताछ कर सकता है। इसके बाद फिजिकल टेस्ट्स और कुछ न्यूरोलॉजिकल टेस्ट्स किए जा सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट्स में, ब्रैडीकिनेसिया के साथ-साथ कठोरता या कम्पन का पता लगाया जा सकता है। आराम करते समय कम्पन होना पीडी के प्रारंभिक लक्षणों में शामिल है।
लेवोडोपा (एल-डोपा) दवाई का उपयोग करके मस्तिष्क में डोपामाइन के स्तर को बढ़ाकर, डॉक्टर रोगी की दवाई के प्रति प्रतिकिया का मूल्याङ्कन करते हैं। इस टेस्ट के आधार पर पीडी के निदान का एक निश्चित परिणाम प्राप्त किया जाता है।
पार्किंसंस रोग के निदान के लिए इमेजिंग टेस्ट जैसे डैटस्कैन (डोपामाइन ट्रांसपोर्टर स्कैन) किया जा सकता है। इसमें मस्तिष्क में डोपामाइन ट्रांसपोर्टरों को देखने के लिए एक रेडियोधर्मी पदार्थ और विशेष कैमरे का उपयोग करता किया जाता है। DaTscan से डोपामाइन न्यूरॉन्स के नुकसान का पता लगाना आसान होता है।
इसके अतिरिक्त मेटाबॉलिक डिजीज का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट, मस्तिष्क की संरचना में असामान्यताओं का पता लगाने के लिए
सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन जैसे न्यूरोइमेजिंग टेस्ट्स किए जा सकते हैं। कुछ पारिवारिक इतिहास वाले मामलों में, जेनेटिक टेस्ट किया जा सकता है।
पार्किंसंस रोग की रोकथाम
पार्किंसंस रोग की रोकथाम के लिए वर्तमान में कोई विशेष रोकथाम रणनीति उपलब्ध नहीं है, लेकिन जीवनशैली में कुछ सकारात्मक बदलाव करने से, जैसे नियमित रूप से एरोबिक व्यायाम करने से, स्वस्थ आहार लेने से, कैफीन के मध्यम सेवन से और पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों के संपर्क से बचने से, इसके विकास के जोखिम को कम किया जा सकता है।
स्वस्थ और संतुलित आहार में फलों, सब्जियों और उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थों को शामिल किया जा सकता है। कुछ शोधों से यह पता चला है कि डेयरी प्रोडक्ट्स के कम सेवन से और एंटीऑक्सिडेंट्स, जो चमकीले रंग के फलों, सब्जियों, चाय और रेड वाइन में पाए जाते हैं, के अधिक सेवन से पीडी के कारण होने वाली कोशिका क्षति से बचा जा सकता है।
पार्किंसंस रोग का उपचार / पार्किंसन डिजीज का इलाज
पार्किंसन डिजीज का वर्तमान में कोई सटीक इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन नॉन-फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल उपचारों द्वारा इसके लक्षणों को कम ज़रूर किया जा सकता है।
1. फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट: पीडी का इलाज करने के लिए फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का उपयोग प्राथमिक उपचार के रूप में किया जा सकता है। आमतौर पर लेवोडोपा और कार्बिडोपा दवाइयों का साथ में उपयोग पार्किंसन डिजीज का इलाज करने के लिए किया जाता है। अन्य दवाइयों में डोपामाइन एगोनिस्ट (जो ब्रेन में डोपामाइन के स्तर को बढ़ाता है), MAO-B इन्हिबिटर्स और COMT इन्हिबिटर्स शामिल हैं।
2. सर्जिकल ट्रीटमेंट: उन्नत पार्किंसन डिजीज का इलाज करने के लिए, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन(DBS) जैसे सर्जिकल ट्रीटमेंट का उपयोग किया जा सकता है। DBS में ब्रेन के स्पेसिफ़िक एरियाज़ में इलेक्ट्रोड प्रत्यारोपित(इम्प्लांट) किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिकल वेव्स उत्पन्न होते हैं, जो असामान्य मस्तिष्क आवेगों(इम्पलसेस) को नियंत्रित करती हैं।
3. नॉन-फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट: नॉन-फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में शरीर की गति को बढ़ाने और मांसपेशियों की ताकत में सुधार करने के लिए फिजियोथेरेपी, डेली लाइफ के कार्यों को करने में मदद के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बोलने और निगलने में होनेवाली दिक्कतों को ठीक करने के लिए स्पीच और लैंग्वेज थेरेपीज़ शामिल हैं।
4. मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच: पार्किंसन डिजीज के लक्षणों को प्रबंधित या कम करने के लिए, न्यूरोलॉजिस्ट, जेरियाट्रिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, डायटीशियन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स, स्पीच थेरेपिस्ट्स, विशेष पीडी नर्सों की एक टीम की आवश्यकता पड़ सकती है।
क्या पार्किंसन डिजीज जीवन के लिए ख़तरा है?
पार्किंसन डिजीज जीवन के लिए ख़तरा नहीं है, लेकिन इस बीमारी के कारण उत्पन्न होनेवाले कॉम्प्लीकेशन्स के कारण रोगी की स्थिति ज़रूर गंभीर हो सकती है, जैसे संतुलन बिगड़ने के कारण गंभीर चोट लग सकती है, निगलने में कठिनाई होने के कारण दम घूँट सकता है, साँस फूलने के कारण बाद में निमोनिया हो सकता है, और इन सभी स्वास्थ्य समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण पीडी रोगियों की मृत्यु हो सकती है।
इसलिए पार्किंसन डिजीज स्वयं जीवन के लिए ख़तरा नहीं है, लेकिन इससे उत्पन्न होनेवाली जटिलताएँ जीवन के लिए ख़तरा अवश्य बन सकती हैं।
पार्किंसन डिजीज के लिए सर्वाइवल रेट्स
पार्किंसन डिजीज को अपनेआप में घातक बीमारी नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी यदि इसका समय पर इलाज नहीं होता है तो घातक रूप अवश्य ले सकता है। पार्किंसन डिजीज से पीड़ित लोगों के लिए यदि सर्वाइवल रेट्स की बात करें तो यह उनके संपूर्ण स्वास्थ्य स्थिति, उम्र और रोग की प्रगति के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। 2018 में किए गए एक बड़े अध्ययन के अनुसार, नर्सिंग होम देखभाल की आवश्यकता पड़ने या मृत्यु की शुरुआत के बाद, पीडी के रोगी लगभग 14 वर्ष तक जी सकते हैं।
पार्किंसन डिजीज के इलाज में लगनेवाला समय
पार्किंसन डिजीज का इलाज लंबे समय तक या जीवन भर चल सकता है। उपचार का उद्देश्य रोग के लक्षणों को नियंत्रित करने के साथ, रोगी को एक बेहतर जीवन प्रदान करना होता है। प्रत्येक रोगी की उपचार के प्रति प्रतिक्रिया बहुत भिन्न हो सकती है, और बीमारी बढ़ने के बाद उपचार का सफ़ल परिणाम प्राप्त करने में अधिक समय लग सकता है।
पार्किंसंस रोग के साथ कैसे लड़ें?
पार्किंसंस रोग के साथ लड़ने में बहुत लंबा समय लग सकता है, क्योंकि यह धीरे-धीरे प्रगति करनेवाली बीमारी है और इसका इलाज भी लंबे समय तक चलता है।
हेल्थकेयर प्रोवाइडर से नियमित जाँच करवाने से, सपोर्ट ग्रुप्स को ज्वाइन करने से, फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी नियमित लेने से पार्किंसंस रोग से सही ढंग से लड़ने में मदद मिल सकती है।
संतुलन बिगड़ने पर गिरने से रोकने के लिए घर की बनावट में बदलाव करने से, चलने के लिए सहायक उपकरणों का उपयोग करने से, कब्ज से बचने और स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए स्वस्थ और संतुलित आहार लेने से काफ़ी हद तक रोगी को पार्किंसंस रोग से लड़ने के लिए प्रेरणा मिल सकती। फिजिकल थेरेपिस्ट द्वारा बताए गए फिजिकल एक्टिविटीज़ को रेग्यूलर करने से शरीर की गति और संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
निष्कर्ष
पार्किंसंस रोग एक जटिल और प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसके लिए एक विशेष चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। पार्किंसंस रोग के लिए वर्तमान में कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को प्रबंधित या कम करने और रोगी को एक बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए कई उपचार उपलब्ध हैं, जिनमें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट और नॉन-फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट शामिल हैं। नियमित जाँच करवाने से और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने से, पार्किंसन रोग का शीघ्र निदान और समय पर उपचार संभव है।
पार्किंसन रोग को और बेहतर तरीके से समझने के लिए वर्तमान में भी शोध जारी हैं। इन शोधों का उद्देश्य, पार्किंसन रोग में न्यूरोनल मृत्यु के सटीक कारण को ढूँढना, बेहतर उपचार ढूँढना और इसका इलाज ढूँढना है।
इस लेख के माध्यम से हमारा आपसे निवेदन है कि पार्किंसन रोग से बचने के लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तभी अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएँगे।
पार्किंसन रोग कैसे होता है? / पार्किंसन रोग क्या है?
पार्किंसंस रोग (पीडी), एक न्यूरोडीजेनेरेटिव डिसऑर्डर है। यह डिसऑर्डर या विकार मुख्य रूप से मस्तिष्क के एक विशिष्ट क्षेत्र में डोपामाइन-उत्पादक, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है, जिसे सबस्टैंटिया नाइग्रा भी कहा जाता है। इस स्थिति का ज़िक्र पहली बार, ब्रिटिश सर्जन डॉ. जेम्स पार्किंसन ने अपनी किताब(जो 1817 में पब्लिश्ड हुई थी) “An Essay on the Shaking Palsy” में की थी। पार्किंसन डिसऑर्डर से लोग तब परिचित होने लगे, जब यह धीरे-धीरे लोगों को अपना शिकार बनाने लगी। वर्तमान में, दुनिया भर में सात से दस मिलियन लोग पार्किंसन डिजीज से प्रभावित होते हैं।
भारत में, आँकड़ों के अनुसार दस लाख लोग पार्किंसंस से पीड़ित हैं। पार्किंसंस से प्रभावित लोग ख़ुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि वह कमज़ोर क्यों महसूस कर रहे हैं, दरअसल यह पार्किंसंस रोग के लक्षण होते हैं।
पार्किंसन डिजीज अक्सर 60 साल या उससे अधिक की उम्र वाले लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन इसके लगभग 4% मामले 50 साल से कम उम्र वाले लोगों में भी मिल सकते हैं। 50 साल से कम उम्र वाले लोगों को होनेवाले पार्किंसन डिसऑर्डर को, यंग-ऑनसेट पार्किंसंस डिजीज कहा जाता है। पार्किंसन डिजीज मानव मस्तिष्क के भीतर होती है, और गति को प्रभावित करने के साथ सोचने की क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है।
पार्किसन बीमारी या पार्किंसन डिजीज, मस्तिष्क के एक हिस्से, सबस्टैंटिया नाइग्रा में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की कमी या मृत्यु के कारण होती है। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स मानव मस्तिष्क को मूवमेंट, स्मृति, अटेंशन, मूड और कई अन्य कार्यों को करने में मदद करता है।
पार्किसन बीमारी जैसे-जैसे बढ़ती है, डोपामाइन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करता है, की कमी होने लगती है, और पार्किंसन डिजीज के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर खुशी, संतुष्टि, प्रेरणा को महसूस कराने के लिए सिग्नल भेजता है। पार्किंसन डिजीज या पार्किंसन रोग क्या है, यह सवाल अब तक सबके सामने एक पहेली बनी हुई है, लेकिन इसके विकसित होने के कारण आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक माने जा सकते हैं।
पार्किंसंस रोग के प्रकार / पार्किसन बीमारी
पार्किंसन डिजीज के कई प्रकार हैं और शुरूआती अवस्था में पार्किंसन डिजीज के लक्षण बहुत ही सूक्ष्म होने के कारण पकड़ में ही नहीं आते हैं। पार्किंसन डिजीज के कुछ प्रकार निम्न हैं:
1. इडियोपैथिक / स्पेसिफ़िक पार्किंसंस डिजीज: इडियोपैथिक या स्पेसिफ़िक पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसंस के सबसे आम प्रकारों में से एक है और इसके अधिकतर मामले पाए जा सकते हैं। इडियोपैथिक या स्पेसिफ़िक पार्किंसंस डिजीज के लक्षण शुरुआत में सूक्ष्म होते हैं, और यह अक्सर शरीर के एक तरफ़ ही विकसित होता है, धीरे-धीरे यह शरीर के दूसरे तरफ़ फैलता है। जैसे-जैसे यह रोग प्रगति करता है, इसके लक्षण भी समय के साथ बढ़ते हैं। पार्किंसन रोग कैसे होता है, इसका अभी तक कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाया है। इसका कारण अज्ञात होने की वजह से इसे “इडियोपैथिक” शब्द दिया गया है।
2. यंग-ऑनसेट पार्किंसंस डिजीज(YOPD): यंग-ऑनसेट पार्किंसंस डिजीज, यंग लोगों में पाया जाता है। आमतौर पर यह डिजीज 50 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को होता है। यंग-ऑनसेट पार्किंसन डिजीज अन्य PD डिजीज की तुलना में कम आम है, और इसके मामले सभी PD डिजीज के मामलों में से लगभग 2% -10% पाए जा सकते है। YOPD धीरे-धीरे प्रगति करनेवाली बीमारी है, जिससे व्यक्ति का प्रोडक्टिव येअर(60-70 वर्ष की उम्र) भी प्रभावित होता है। YOPD के लक्षण भी अक्सर इडियोपैथिक के लक्षण जैसे ही होते हैं, लेकिन इसके लक्षण धीरे-धीरे प्रगति करते हैं। वाईओपीडी के लक्षण, शुरुआत में डिस्टोनिया रोग(न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर) के रूप में दिख सकते हैं।
3. पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम / एटिपिकल पार्किंसनिज़्म: पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम या एटिपिकल पार्किंसनिज़्म, न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों का एक समूह है जो पार्किंसंस रोग के कुछ लक्षणों के साथ प्रकट होता है, लेकिन इसकी और भी विशेषताएँ होती हैं और यह अधिक तेज़ी से प्रगति करता है। पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम में, मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी (एमएसए), प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी (पीएसपी), कॉर्टिकोबैसल डीजनरेशन (सीबीडी), और लेवी बॉडीज के साथ डिमेंशिया (डीएलबी) शामिल हैं। मानक पीडी दवाइयों का असर इन स्थितियों पर कुछ ख़ास नहीं होता है, और रोगी की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है।
पार्किंसन डिजीज के लक्षण / पार्किसन बीमारी के लक्षण
पार्किंसन डिजीज के लक्षणों को, मोटर और नॉन-मोटर श्रेणियों(कैटेगरी) में बाँटा गया है। पार्किंसन डिजीज के लक्षण, शरीर के एक ओर से शुरू होते हैं और धीरे-धीरे दूसरी ओर को प्रभावित करते हैं। शुरुआत में पार्किंसन डिजीज के लक्षण सूक्ष्म होते हैं। मोटर लक्षण को अधिकांश, पार्किंसन डिजीज के लक्षण माने जाते हैं और वह लक्षण इस प्रकार हैं:
1. कँपकँपी: कँपकँपी, पार्किंसन डिजीज के लक्षण में से एक लक्षण है और यह शुरूआती लक्षण है। यह लक्षण हाथ या उँगलियों में प्रकट हो सकता है। पार्किंसन डिजीज का एक लक्षण, आराम करते समय हाथ में होनेवाली कँपकँपी है। पार्किंसन के हर केस में यह आवश्यक नहीं है कि कँपकँपी जैसे लक्षण प्रकट हों।
2. ब्रैडीकिनेसिया (गति का धीमा होना): ब्रैडीकिनेसिया भी पार्किंसन डिजीज के लक्षण में से एक है। पार्किंसन डिजीज के बढ़ने के साथ, रोगी के कार्य करने की गति भी धीमी हो जाती है, और उसे सरल कार्यों को करने में भी कठिनाई होने लगती है।
3. मांसपेशियों का कठोर होना: पार्किंसन डिजीज के लक्षण में, मांसपेशियों का कठोर होना शामिल है। इस बीमारी में शरीर के किसी भी हिस्से में मांसपेशियाँ कठोर हो सकती हैं। मांसपेशियों की कठोरता, गति की सीमा को सीमित करने और मांसपेशियों में दर्द का कारण बन सकती है।
4. संतुलन और समन्वय संबंधित समस्याएँ: पार्किंसन डिजीज के बढ़ने से संतुलन और समन्वय संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। संतुलन और समन्वय संबंधित समस्याएँ भी, पार्किंसन डिजीज के लक्षण में शामिल हैं।
पार्किंसंस के नॉन-मोटर लक्षण चलने-फिरने जैसी गतिविधियों से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन मोटर लक्षणों की तुलना में दैनिक जीवन में अधिक तनाव और निराशा का कारण बन सकते हैं। पार्किंसंस के नॉन-मोटर, मोटर लक्षणों से पहले प्रकट हो सकते हैं, और कभी-कभी अधिक दिखाई देने वाले शारीरिक लक्षणों से वर्षों पहले प्रकट होते हैं, इसलिए इन्हें प्री-मोटर लक्षण भी कहा जाता है। सूँघने की क्षमता का कम होना, डिप्रेशन और कॉन्स्टिपेशन जैसे लक्षण वास्तविक निदान से वर्षों पहले प्रकट हो सकते हैं। पीडी के गैर-मोटर लक्षणों में शामिल हैं:
1. मूड डिसऑर्डर: पार्किंसन डिजीज के लक्षण में मूड में बदलाव होना शामिल है। पार्किंसन रोग में व्यक्ति डिप्रेशन या एंग्जायटी का अनुभव कर सकता है।
2. नींद नहीं आना: पीडी में नींद संबंधित समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। नींद में कमी होना पार्किंसन डिजीज के लक्षण में से एक लक्षण है।
3. संज्ञानात्मक परिवर्तन: पार्किंसन डिजीज में, संज्ञानात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे- स्मृति, ध्यान, कार्यकारी कार्य (योजना, समस्या-समाधान), और नेत्र संबंधी कौशल, पार्किंसन डिजीज के लक्षण में शामिल हैं।
4. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम (एएनएस) की शिथिलता: पार्किंसंस के कुछ गैर-मोटर लक्षण, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, शरीर द्वारा ऑटोमेटिकली किए जाने वाले कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे रक्तचाप, हृदय गति, पसीना आदि। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में परिवर्तन होने पर, कब्ज, मूत्र, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन (खड़े होने पर रक्तचाप में गिरावट), और यौन रोग संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
5. सूँघने की क्षमता कम होना: पीडी के कई केसेस में, मोटर लक्षणों की शुरुआत से वर्षों पहले सूँघने की क्षमता कम होने लगती है। सूँघने की क्षमता कम हो जाना, पार्किंसन डिजीज के लक्षण में शामिल हैं।
पार्किंसंस रोग के कारण / पार्किंसंस रोग कैसे होता है?
पार्किंसंस रोग का सटीक कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है, लेकिन इसके विकास के कारणों में आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक शामिल हो सकते हैं।
1. आनुवंशिक कारक: पार्किंसंस रोग के लगभग 10% -15% मामलों में जेनेटिक फैक्टर्स जैसे कारक, कारण पाए जा सकता हैं। पार्किंसंस रोग के विकास के कारणों में एसएनसीए, एलआरआरके2, पीआरकेएन, पिंक1 और डीजे-1 जैसे विशिष्ट जीनों में उत्परिवर्तन शामिल हैं।
2. पर्यावरणीय कारक: पार्किंसंस रोग के कारणों में, कुछ पर्यावरणीय कारक जैसे, ग्रामीण जीवन, कुऍं के पानी का संपर्क, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स के जोखिम शामिल हो सकते हैं। यह जोखिम कारक आनुवंशिक रूप से अतिसंवेदनशील व्यक्तियों में भी पीडी के विकास का कारण बन सकते हैं।
पार्किंसन डिजीज के चरण
पार्किंसंस रोग के चरणों को पाँच चरणों में विभाजित किया गया है। चरणों की जानकारी से पीडी रोग की प्रगति का पता चल सकता है, और आगे उपचार के लिए प्लानिंग भी जा सकती है। पार्किंसंस रोग के चरण निम्न हैं:
1. चरण I: पार्किंसंस के पहले चरण में, हल्के लक्षण प्रकट हो सकते हैं, जैसे शरीर का केवल एक तरफ़ या एक ओर प्रभावित हो सकता है। पहले चरण के लक्षणों में, एक हाथ में हल्का सा कंपन, मुद्रा में बदलाव और चेहरे के भाव में बदलाव शामिल हैं।
2. चरण II: दूसरे चरण में, शरीर का दोनों तरफ़ का हिस्सा प्रभावित होना शुरूहो जाता है, लेकिन संतुलन में कोई हानि नहीं होती है। इस चरण के लक्षणों में शरीर के दोनों तरफ़ कठोरता, कँपकँपी और चेहरे की अभिव्यक्ति में बदलाव शामिल हो सकते हैं।
3. चरण III: इस चरण में गति धीमी होने के साथ, संतुलन की हानि का अनुभव भी किया जा सकता है। कपड़े पहनने और खाने जैसे कार्यों में दिक्कत हो सकती है।
4. चरण IV: पीडी के चौथे चरण में चलने और खड़े होने की क्षमता कम हो सकती है। दैनिक जीवन में कार्यों को करने में कठिनाई का अनुभव किया जा सकता है।
5. चरण V: यह चरण पार्किंसंस का अंतिम चरण और सबसे उन्नत चरण होता है। इस चरण में, सभी दैनिक गतिविधियों को करने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त मतिभ्रम और भ्रम जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस चरण में रोगी की विशेष चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है।
पार्किंसंस रोग का निदान / पार्किसन बीमारी का निदान
पार्किंसंस रोग के निदान के लिए सबसे पहले डॉक्टर, रोगी के चिकित्सा इतिहास और रोग के लक्षणों के बारे में पूछताछ कर सकता है। इसके बाद फिजिकल टेस्ट्स और कुछ न्यूरोलॉजिकल टेस्ट्स किए जा सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट्स में, ब्रैडीकिनेसिया के साथ-साथ कठोरता या कम्पन का पता लगाया जा सकता है। आराम करते समय कम्पन होना पीडी के प्रारंभिक लक्षणों में शामिल है।
लेवोडोपा (एल-डोपा) दवाई का उपयोग करके मस्तिष्क में डोपामाइन के स्तर को बढ़ाकर, डॉक्टर रोगी की दवाई के प्रति प्रतिकिया का मूल्याङ्कन करते हैं। इस टेस्ट के आधार पर पीडी के निदान का एक निश्चित परिणाम प्राप्त किया जाता है।
पार्किंसंस रोग के निदान के लिए इमेजिंग टेस्ट जैसे डैटस्कैन (डोपामाइन ट्रांसपोर्टर स्कैन) किया जा सकता है। इसमें मस्तिष्क में डोपामाइन ट्रांसपोर्टरों को देखने के लिए एक रेडियोधर्मी पदार्थ और विशेष कैमरे का उपयोग करता किया जाता है। DaTscan से डोपामाइन न्यूरॉन्स के नुकसान का पता लगाना आसान होता है।
इसके अतिरिक्त मेटाबॉलिक डिजीज का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट, मस्तिष्क की संरचना में असामान्यताओं का पता लगाने के लिए
सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन जैसे न्यूरोइमेजिंग टेस्ट्स किए जा सकते हैं। कुछ पारिवारिक इतिहास वाले मामलों में, जेनेटिक टेस्ट किया जा सकता है।
पार्किंसंस रोग की रोकथाम / पार्किसन बीमारी की रोकथाम
पार्किंसंस रोग की रोकथाम के लिए वर्तमान में कोई विशेष रोकथाम रणनीति उपलब्ध नहीं है, लेकिन जीवनशैली में कुछ सकारात्मक बदलाव करने से, जैसे नियमित रूप से एरोबिक व्यायाम करने से, स्वस्थ आहार लेने से, कैफीन के मध्यम सेवन से और पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों के संपर्क से बचने से, इसके विकास के जोखिम को कम किया जा सकता है।
स्वस्थ और संतुलित आहार में फलों, सब्जियों और उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थों को शामिल किया जा सकता है। कुछ शोधों से यह पता चला है कि डेयरी प्रोडक्ट्स के कम सेवन से और एंटीऑक्सिडेंट्स, जो चमकीले रंग के फलों, सब्जियों, चाय और रेड वाइन में पाए जाते हैं, के अधिक सेवन से पीडी के कारण होने वाली कोशिका क्षति से बचा जा सकता है।
पार्किंसंस रोग का उपचार / पार्किंसन डिजीज का इलाज
पार्किंसन डिजीज का वर्तमान में कोई सटीक इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन नॉन-फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल उपचारों द्वारा इसके लक्षणों को कम ज़रूर किया जा सकता है।
1. फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट: पीडी का इलाज करने के लिए फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का उपयोग प्राथमिक उपचार के रूप में किया जा सकता है। आमतौर पर लेवोडोपा और कार्बिडोपा दवाइयों का साथ में उपयोग पार्किंसन डिजीज का इलाज करने के लिए किया जाता है। अन्य दवाइयों में डोपामाइन एगोनिस्ट (जो ब्रेन में डोपामाइन के स्तर को बढ़ाता है), MAO-B इन्हिबिटर्स और COMT इन्हिबिटर्स शामिल हैं।
2. सर्जिकल ट्रीटमेंट: उन्नत पार्किंसन डिजीज का इलाज करने के लिए, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन(DBS) जैसे सर्जिकल ट्रीटमेंट का उपयोग किया जा सकता है। DBS में ब्रेन के स्पेसिफ़िक एरियाज़ में इलेक्ट्रोड प्रत्यारोपित(इम्प्लांट) किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिकल वेव्स उत्पन्न होते हैं, जो असामान्य मस्तिष्क आवेगों(इम्पलसेस) को नियंत्रित करती हैं।
3. नॉन-फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट: नॉन-फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में शरीर की गति को बढ़ाने और मांसपेशियों की ताकत में सुधार करने के लिए फिजियोथेरेपी, डेली लाइफ के कार्यों को करने में मदद के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बोलने और निगलने में होनेवाली दिक्कतों को ठीक करने के लिए स्पीच और लैंग्वेज थेरेपीज़ शामिल हैं।
4. मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच: पार्किंसन डिजीज के लक्षणों को प्रबंधित या कम करने के लिए, न्यूरोलॉजिस्ट, जेरियाट्रिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, डायटीशियन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स, स्पीच थेरेपिस्ट्स, विशेष पीडी नर्सों की एक टीम की आवश्यकता पड़ सकती है।
क्या पार्किंसन डिजीज जीवन के लिए ख़तरा है?
पार्किंसन डिजीज जीवन के लिए ख़तरा नहीं है, लेकिन इस बीमारी के कारण उत्पन्न होनेवाले कॉम्प्लीकेशन्स के कारण रोगी की स्थिति ज़रूर गंभीर हो सकती है, जैसे संतुलन बिगड़ने के कारण गंभीर चोट लग सकती है, निगलने में कठिनाई होने के कारण दम घूँट सकता है, साँस फूलने के कारण बाद में निमोनिया हो सकता है, और इन सभी स्वास्थ्य समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण पीडी रोगियों की मृत्यु हो सकती है।
इसलिए पार्किंसन डिजीज स्वयं जीवन के लिए ख़तरा नहीं है, लेकिन इससे उत्पन्न होनेवाली जटिलताएँ जीवन के लिए ख़तरा अवश्य बन सकती हैं।
पार्किंसन डिजीज के लिए सर्वाइवल रेट्स
पार्किंसन डिजीज को अपनेआप में घातक बीमारी नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी यदि इसका समय पर इलाज नहीं होता है तो घातक रूप अवश्य ले सकता है। पार्किंसन डिजीज से पीड़ित लोगों के लिए यदि सर्वाइवल रेट्स की बात करें तो यह उनके संपूर्ण स्वास्थ्य स्थिति, उम्र और रोग की प्रगति के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। 2018 में किए गए एक बड़े अध्ययन के अनुसार, नर्सिंग होम देखभाल की आवश्यकता पड़ने या मृत्यु की शुरुआत के बाद, पीडी के रोगी लगभग 14 वर्ष तक जी सकते हैं।
पार्किंसन डिजीज के इलाज में लगनेवाला समय
पार्किंसन डिजीज का इलाज लंबे समय तक या जीवन भर चल सकता है। उपचार का उद्देश्य रोग के लक्षणों को नियंत्रित करने के साथ, रोगी को एक बेहतर जीवन प्रदान करना होता है। प्रत्येक रोगी की उपचार के प्रति प्रतिक्रिया बहुत भिन्न हो सकती है, और बीमारी बढ़ने के बाद उपचार का सफ़ल परिणाम प्राप्त करने में अधिक समय लग सकता है।
पार्किंसंस रोग के साथ कैसे लड़ें?
पार्किंसंस रोग के साथ लड़ने में बहुत लंबा समय लग सकता है, क्योंकि यह धीरे-धीरे प्रगति करनेवाली बीमारी है और इसका इलाज भी लंबे समय तक चलता है।
हेल्थकेयर प्रोवाइडर से नियमित जाँच करवाने से, सपोर्ट ग्रुप्स को ज्वाइन करने से, फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी नियमित लेने से पार्किंसंस रोग से सही ढंग से लड़ने में मदद मिल सकती है।
संतुलन बिगड़ने पर गिरने से रोकने के लिए घर की बनावट में बदलाव करने से, चलने के लिए सहायक उपकरणों का उपयोग करने से, कब्ज से बचने और स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए स्वस्थ और संतुलित आहार लेने से काफ़ी हद तक रोगी को पार्किंसंस रोग से लड़ने के लिए प्रेरणा मिल सकती। फिजिकल थेरेपिस्ट द्वारा बताए गए फिजिकल एक्टिविटीज़ को रेग्यूलर करने से शरीर की गति और संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
निष्कर्ष
पार्किंसंस रोग एक जटिल और प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसके लिए एक विशेष चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। पार्किंसंस रोग के लिए वर्तमान में कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को प्रबंधित या कम करने और रोगी को एक बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए कई उपचार उपलब्ध हैं, जिनमें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट और नॉन-फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट शामिल हैं। नियमित जाँच करवाने से और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने से, पार्किंसन रोग का शीघ्र निदान और समय पर उपचार संभव है।
पार्किंसन रोग को और बेहतर तरीके से समझने के लिए वर्तमान में भी शोध जारी हैं। इन शोधों का उद्देश्य, पार्किंसन रोग में न्यूरोनल मृत्यु के सटीक कारण को ढूँढना, बेहतर उपचार ढूँढना और इसका इलाज ढूँढना है।
इस लेख के माध्यम से हमारा आपसे निवेदन है कि पार्किंसन रोग से बचने के लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तभी अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएँगे।
कई बार ख़ुद की सेविंग्स से इलाज के लिए पैसे जुटाना मुश्किल हो जाता है।
ऐसे केसेस में जहाँ इलाज का खर्च बहुत अधिक हो, इम्पैक्ट गुरु जैसी वेबसाइट पर फंडरेज़िंग के लिए एक बहुत ही शानदार तरीका उपलब्ध है।