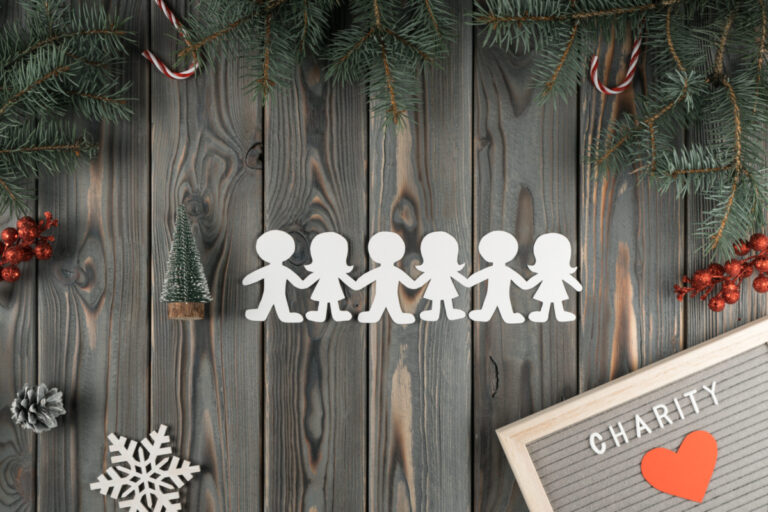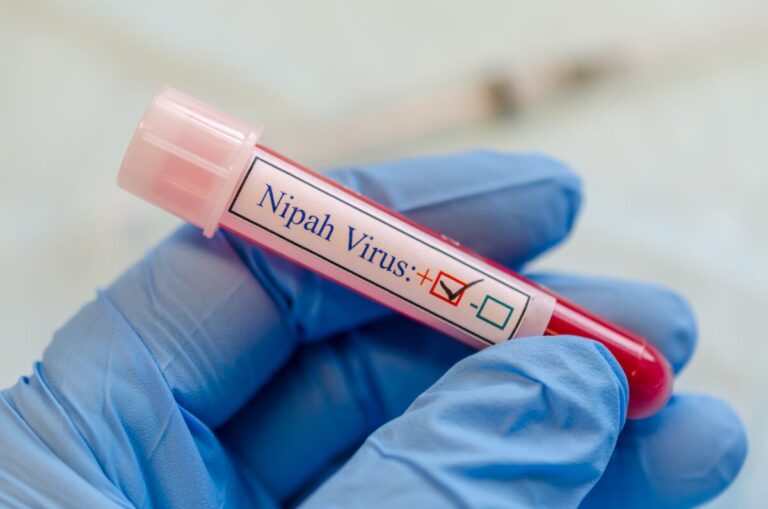वायरल फीवर या वायरल बुखार, भारत में एक आम स्वास्थ्य चिंता का विषय है, और यह सभी उम्र और क्षेत्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। यदि यह समझने का प्रयास करें कि वायरल फीवर क्या है और वायरल फीवर क्यों होता है, तो वायरल फीवर एक प्रकार का बुखार है, जिसमें शरीर का तापमान बढ़ जाता है, और यह विभिन्न प्रकार के वायरल रोगजनकों (Viral Pathogens) के शरीर पर आक्रमण करने के कारण होता है। सरल शब्दों में समझें, तो वायरल बुखार विभिन्न प्रकार के वायरस के संक्रमण के कारण होता है, जैसे इन्फ्लूएंजा वायरस, डेंगू वायरस, चिकनगुनिया और SARS-CoV-2 वायरस (COVID-19 के लिए ज़िम्मेदार)। यह वायरस मच्छरों, श्वसन बूँदों (Respiratory Droplets) और संक्रमित व्यक्तियों (Infected Persons) के सीधे संपर्क में आने के साथ विभिन्न वाहकों के माध्यम से फैल सकते हैं। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, जहाँ अत्यधिक गंदगी होती है, वहाँ वायरल बुखार बहुत तेज़ी से फैल सकता है।
वायरस सूक्ष्म संक्रामक एजेंट होते हैं, और यह शरीर की कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है और बुखार के साथ विभिन्न लक्षण पैदा होते हैं।
भारत में, जहाँ किसी बीमारी की प्रगति के लिए पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक कारक ज़िम्मेदार हो सकते हैं, वहाँ वायरल फीवर के प्रभावी प्रबंधन और रोकथाम के लिए, वायरल फीवर को समझना आवश्यक है। इस लेख के माध्यम से हमारा उद्देश्य, भारत के लोगों को वायरल फीवर या वायरल बुखार के प्रकारों, लक्षणों, कारणों, निदान, रोकथाम रणनीतियों, उपचार विकल्पों और सर्वाइवल रेट के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करना है।
Table of Contents
- वायरल फीवर के प्रकार / वायरल बुखार के प्रकार
- वायरल फीवर के लक्षण / वायरल बुखार के लक्षण
- वायरल फीवर क्यों होता है? / वायरल बुखार क्यों होता है?
- वायरल बुखार का निदान
- वायरल बुखार की रोकथाम
- वायरल बुखार की दवा / वायरल बुखार का रामबाण इलाज
- वायरल बुखार के लिए सर्वाइवल रेट
- निष्कर्ष
- वायरल बुखार के लक्षण और उपाय या वायरल फीवर के लक्षण और उपचार संक्षेप में
वायरल फीवर के प्रकार / वायरल बुखार के प्रकार

वायरल बुखार या वायरल फीवर, विभिन्न वायरल इंफेक्शंस के कारण होता है, और इसमें कई प्रकार के लक्षण प्रकट हो सकते हैं। यहाँ वायरल फीवर के कुछ सामान्य प्रकारों का वर्णन किया गया है:
1. इन्फ्लूएंजा (फ्लू): इन्फ्लूएंजा वायरस के कारण होने वाले फ्लू में, आमतौर पर तेज़ बुखार, शरीर में दर्द, थकान, खाँसी, गले में खराश जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं, साथ ही कभी-कभी नाक बह सकती है या नाक बंद रह सकता है। इन्फ्लूएंजा फ्लू बढ़ने पर, व्यक्ति निमोनिया जैसी बीमारियों का शिकार हो सकता है।
2. डेंगू बुखार: डेंगू मच्छरों या एडीज मच्छरों के कारण होनेवाले डेंगू बुखार में, तेज़ बुखार, गंभीर सिरदर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, दाने और कभी-कभी रक्तस्राव जैसे लक्षण प्रकट हो सकते हैं। डेंगू बुखार के बढ़ने पर, व्यक्ति को डेंगू रक्तस्रावी बुखार (Dengue Hemorrhagic Fever) या डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है।
3. चिकनगुनिया: एडीज मच्छरों के कारण होनेवाले चिकनगुनिया में, बुखार, जोड़ों में गंभीर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द और दाने जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। चिकनगुनिया में, जोड़ों का दर्द लंबे समय तक रह सकता है, जिससे स्वास्थ्य स्थिति अधिक दुर्बल हो सकती है।
4. जीका वायरस: जीका वायरस, एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। इस रोग में हल्के बुखार, दाने, जोड़ों में दर्द और कंजंक्टिवाइटिस (आँखों की बीमारी, जिसमें आँखें लाल हो जाती हैं) जैसे लक्षण प्रकट हो सकते हैं। यदि गर्भवती महिलाओं को जीका वायरस हो जाता है, तो भ्रूण भी संक्रमित हो सकता है, जिससे बच्चा छोटे आकार के सिर और दिमाग के साथ पैदा होता है।
5. COVID-19: नोवल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के कारण होने वाले, COVID-19 में बुखार, खाँसी, साँस लेने में दिक्कत, थकान, स्वाद या गंध की हानि (Loss of Taste or Smell) के साथ कई अन्य लक्षण पैदा हो सकते हैं।
6. रेबीज: संक्रमित जानवर के काटने से होने वाले रेबीज में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और अंततः न्यूरोलॉजिकल लक्षण पैदा हो सकते हैं।
7. येलो फीवर: मच्छरों के कारण होनेवाले, येलो फीवर, फीवर, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, मतली का कारण बन सकता है। येलो फीवर के गंभीर चरणों में, व्यक्ति में पीलिया, रक्तस्राव और अंग विफलता (Organ Failure) जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं।
8. खसरा: खसरा या मीजल्स, मीजल्स वायरस के कारण होता है। इस रोग में तेज़ बुखार, खाँसी, नाक बहना और मुँह के अंदर सफेद धब्बे होना जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। यह रोग अधिकतर छोटे बच्चों को अपनी चपेट में लेता है।
9. हेपेटाइटिस ए: यह एक लिवर डिजीज है, जो हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है। इस प्रकार के वायरल संक्रमण में, बुखार, थकान, भूख में कमी, मतली और पीलिया जैसे लक्षण प्रकट हो सकते हैं।
10. एचआईवी/एड्स: ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV) संक्रमण के कारण एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम (AIDS) हो सकता है, जिससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। हालाँकि इसमें हमेशा बुखार जैसे लक्षण पैदा नहीं होते हैं, लेकिन अवसरवादी संक्रमण (Opportunistic Infections) के कारण यह रोग विभिन्न लक्षणों के साथ प्रकट हो सकता है। अवसरवादी संक्रमण (Opportunistic Infections) का अर्थ होता है, ऐसा संक्रमण हैं जो स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों की तुलना में कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में अधिक बार हो सकते हैं या अधिक गंभीर होते हैं।
वायरल फीवर या वायरल बुखार के प्रकारों के बारे में जानकारी होने से, चिकित्सकों को रोगी के उपचार के लिए, एक बेहतर उपचार योजना बनाने में सहायता मिल सकती है।
वायरल फीवर के लक्षण / वायरल बुखार के लक्षण
वायरल फीवर के लक्षण या वायरल बुखार के लक्षण, संक्रमण पैदा करने वाले विभिन्न वायरस के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। शोधों के आधार पर कुछ पहचान किए गए वायरल फीवर के लक्षण निम्न हैं:
1. बुखार: शरीर के तापमान में अचानक वृद्धि होना या बुखार होना वायरल फीवर के लक्षण या वायरल बुखार के लक्षण में से एक लक्षण है। वायरल फीवर में, बुखार के साथ ठंड भी लग सकती है और पसीना भी आ सकता है।
2. शरीर में दर्द और थकान: शरीर में दर्द और थकान रहना, वायरल फीवर के लक्षण या वायरल बुखार के लक्षण में शामिल हैं।
3. श्वसन लक्षण: खाँसी, गले में खराश और नाक बहना, यह सभी वायरल फीवर के लक्षण या वायरल बुखार के लक्षण हैं।
4. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण: मतली, उल्टी और दस्त जैसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएँ भी, वायरल फीवर के लक्षण या वायरल बुखार के लक्षण में सम्मिलित हैं।
5. दाने: कुछ वायरल संक्रमण जैसे डेंगू और चिकनगुनिया में, एक विशेष दाना प्रकट हो सकता है।
6. जोड़ों का दर्द: जोड़ों में गंभीर दर्द होना भी वायरल फीवर के लक्षण या वायरल बुखार के लक्षण में से एक है।
7. सिरदर्द: सिरदर्द होना भी वायरल फीवर के लक्षण में शामिल है।
वायरल फीवर क्यों होता है? / वायरल बुखार क्यों होता है?
वायरल फीवर या वायरल बुखार को वायरल इंफेक्शन के रूप में भी जाना जाता है। वायरल फीवर विभिन्न प्रकार के वायरस के कारण उत्पन्न होनेवाली एक सामान्य चिकित्सा स्थिति है। इसमें आमतौर पर शरीर का तापमान बढ़ जाता है, साथ ही थकान, शरीर में दर्द, सिरदर्द, खाँसी और कंजेशन जैसे लक्षण प्रकट हो सकते हैं। वायरल फीवर या वायरल बुखार के कुछ प्रमुख कारणों में शामिल हैं:
1. वायरल रोगजनक / वायरल रोगाणु (Viral Pathogens): वायरल बुखार विभिन्न प्रकार के वायरस के कारण हो सकता है, जिनमें इन्फ्लूएंजा वायरस, राइनोवायरस (सामान्य सर्दी का कारण), एडेनोवायरस इत्यादि शामिल हैं। यह वायरस शरीर पर आक्रमण करते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के कारण बुखार जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं।
2. संचरण (Transmission): वायरल इंफेक्शन, किसी संक्रमित व्यक्ति (Infected Person) के सीधे संपर्क में आने से, खाँसी और छींक से निकलने वाली बूँदों के माध्यम से और दूषित सतहों (Contaminated Surfaces) को छूकर चेहरे को छूने से फैल सकते हैं।
3. कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली (Weakened Immune System): कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों को आसानी से वायरल इंफेक्शन हो सकता है।
4. मौसम में परिवर्तन (Seasonal Changes): मौसमों में परिवर्तन होने के कारण जैसे गर्म से ठंडे या बरसात के मौसम में बदलाव होने से भी वायरल संक्रमण फैलने का ख़तरा बढ़ सकता है।
5. वायरस का उत्परिवर्तन (Virus Mutation): जब वायरस समय के साथ उत्परिवर्तन (Mutation) करते हैं, तब वायरस के नए प्रकार उभर सकते हैं जो गंभीर संक्रमण का कारण बन सकते हैं।
6. टीकाकरण की कमी (Lack of Vaccination): टीका नहीं लगवाने से व्यक्ति बहुत तरह के वायरल बीमारियों को न्यौता दे सकता है। टीके की मदद से कई वायरल बीमारियों को रोका या उनकी गंभीरता को कम किया जा सकता है।
7. वैश्विक यात्रा और शहरीकरण (Global Travel and Urbanization): तेज़ी से शहरीकरण के कारण शहरों में भीड़ जमा होने से वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। इसके अतिरिक्त बढ़ती यात्रा के कारण भी वायरस आसानी से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैल सकता है। वायरस के फैलने से वायरल फीवर के मामलों में तेज़ी से वृद्धि हो सकती है।
8. खराब स्वच्छता प्रथाएँ (Poor Hygiene Practices): नियमित रूप से हाथ नहीं धोने से और स्वच्छता नहीं बनाए रखने से, वायरस आँखों, नाक या मुँह के माध्यम से शरीर के भीतर प्रवेश कर सकता है, जिससे वायरल इंफेक्शन का ख़तरा बढ़ सकता है।
9. भीड़-भाड़ वाली सेटिंग (Crowded Setting): गंदगी और घनी आबादी वाले इलाकों में रहनेवाले लोग, आसानी से रोगजनकों (Viral Pathogens) के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे वह वायरल बुखार या वायरल फीवर से पीड़ित हो सकते हैं।
10. वायरल शेडिंग (Viral Shedding): संक्रमित व्यक्ति, वायरल बुखार के लक्षणों के कम होने के बाद भी यदि किसी के संपर्क में आता है, तो उससे दूसरे व्यक्ति में वायरस फैल सकता है। इसलिए संक्रमित व्यक्ति को पूर्ण रूप से ठीक होने के बाद ही किसी अन्य व्यक्ति से मिलना चाहिए।
अच्छी स्वच्छता बनाए रखने से, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से, टीकाकरण कराने से और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचने से, वायरल बुखार की रोकथाम संभव है।
वायरल बुखार का निदान
वायरल बुखार के नैदानिक प्रक्रिया में नैदानिक मूल्यांकन (Clinical Evaluation), रोगी का चिकित्सा इतिहास और प्रयोगशाला परीक्षण (Laboratory Tests) शामिल हैं। वायरल बुखार का निदान निम्न प्रकार से किया जा सकता है:
1. नैदानिक मूल्यांकन (Clinical Asessment): वायरल बुखार या वायरल फीवर का निदान करने के लिए डॉक्टर रोगी के शरीर में, वायरल फीवर के लक्षणों की जाँच कर सकता है। इन लक्षणों में, बुखार, शरीर में दर्द, सिरदर्द, थकान और श्वसन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर रोगी से, लक्षणों के शुरुआत के समय बारे में, यात्रा से संबंधित और वह पूर्व में वायरस के संपर्क में आया है या नहीं, इसके बारे में पूछ सकता है।
2. शारीरिक परीक्षण (Physical Exam): एक संपूर्ण शारीरिक परीक्षण के द्वारा, वायरल इन्फेक्शन से संबंधित लक्षणों की पहचान करने में मदद मिल सकती है।
3. प्रयोगशाला परीक्षण (Laboratory Tests): वायरल बुखार या वायरल फीवर का निदान लक्षणों के आधार पर किया जाता है। कुछ प्रयोगशाला परीक्षणों द्वारा, वायरल फीवर के निदान का एक निश्चित परिणाम प्राप्त किया जा सकता है:
A. रक्त परीक्षण (Blood Tests): ब्लड टेस्ट की मदद से वायरल बुखार से संबंधित लक्षणों की पहचान करने में मदद मिल सकती है।
B. वायरल परीक्षण (Viral Tests): पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन (PCR) टेस्ट या एंटीजन टेस्ट के द्वारा, रोगी के खून, श्वसन स्राव (Respiratory Secretions) या शरीर के अन्य तरल पदार्थों में विशिष्ट वायरस की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। इन वायरल टेस्ट्स के द्वारा, इन्फ्लूएंजा, डेंगू या COVID-19 जैसे आम वायरल इंफेक्शंस का पता लगाया जा सकता है।
C. सीरोलॉजी परीक्षण (Serology Test): यह एक ब्लड टेस्ट है, जिससे वायरल संक्रमण के कारण इम्यून सिस्टम के द्वारा निर्माण किए गए एंटीबॉडीज का पता लगाया जा सकता है। यह एंटीबॉडीज़ इम्यून सिस्टम के द्वारा, शरीर की बाहरी रोगाणु या एंटिजेन से सुरक्षा करने के लिए प्रोड्यूज़ किए जाते हैं। सीरोलॉजी टेस्ट के द्वारा, कुछ वायरस के पिछले संपर्क का भी पता लगाया जा सकता है।
4. इमेजिंग टेस्ट्स: कुछ मामलों में एक्स-रे या सीटी स्कैन जैसे इमेजिंग टेस्ट्स की मदद से छाती में श्वसन लक्षणों की गंभीरता का पता लगाया जा सकता है।
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वायरल बुखार कोई विशिष्ट बीमारी नहीं बल्कि एक लक्षण है, जो शरीर पर विभिन्न प्रकार के वायरस के आक्रमण करने के कारण उत्पन्न हो सकता है। कई बार वायरल इंफेक्शन के लक्षणों को किसी अन्य स्थिति से संबंधित मानकर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है, लेकिन लक्षणों के बने रहने पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करना आवश्यक है, और शंका दूर करने के लिए परीक्षण करवाना भी आवश्यक है।
वायरल बुखार की रोकथाम
जिस प्रकार भारत में तेज़ी से वायरल बुखार के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, इससे यह तो साफ है कि शीघ्र ही इसकी रोकथाम आवश्यक है। वायरल बुखार को रोकने के तरीकों का वर्णन नीचे किया गया है:
1. मच्छर नियंत्रण: जैसा कि हमें ज्ञात है कि वायरल बुखार मच्छरों के द्वारा फैलता है, इसलिए मच्छर नियंत्रण आवश्यक है। मच्छर नियंत्रण के लिए, कंटेनरों, गटरों और अन्य जगहों से रुके हुए पानी को साफ करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, मच्छरदानी, रिपेलेंट का उपयोग करने और सुरक्षात्मक कपड़े पहनने से भी मच्छरों से बचा जा सकता है।
2. अच्छी स्वच्छता और नियमित सफाई: अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने से और नियमित रूप से अपने रहने की जगहों की सफाई करने से, वायरस के प्रसार को रोकने में बहुत हद तक मदद मिल सकती है।
3. टीकाकरण: वायरल बुखार को रोकने में टीकाकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्फ्लूएंजा, डेंगू और अन्य बीमारियों के लिए टीके उपलब्ध हैं। सुरक्षित रहने के लिए अनुशंसित टीकाकरण कार्यक्रम का पालन करना आवश्यक है।
4. भीड़-भाड़ वाले इलाकों से बचना: व्यक्ति भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में अधिकतर वायरस के संपर्क में आ सकता है, जिससे वह वायरल बुखार का शिकार हो सकता है। इसलिए वायरल बुखार या अन्य वायरल बीमारियों से बचने के लिए भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से बचना आवश्यक है।
5. सुरक्षित भोजन और पानी: स्वच्छ और स्वस्थ भोजन करने से और शुद्ध पानी पीने से, पानी के द्वारा फैलनेवाले इंफेक्शंस से बचा जा सकता है।
6. व्यक्तिगत सुरक्षा: बाहर जाते समय लॉन्ग स्लीव्स वाले कपड़े और फुल पैंट जैसे सुरक्षात्मक कपड़े पहनने से, मच्छरों और अन्य संभावित वैक्टरों के संपर्क में आने से बचा जा सकता है।
7. चिकित्सा सहायता लेना: बुखार, शरीर में दर्द और अन्य फ्लू जैसे लक्षण महसूस करने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने से भी वायरल फीवर या अन्य वायरल बीमारियों से बचने में मदद मिल सकती है।
8. सामुदायिक जागरूकता: कम्युनिटीज़ को वायरल बीमारियों के लक्षण, कारण, उपचार, रोकथाम रणनीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करने से भी, बहुत हद तक वायरल बुखार के प्रसार को कम किया जा सकता है।
9. यात्रा सावधानियाँ: वायरल बीमारियों या बुखार वाले क्षेत्रों में, यात्रा के दौरान मच्छरदानी, रिपेलेंट का उपयोग करने से और स्थानीय चिकित्सक से सलाह लेने से, वायरल बुखार से बचा जा सकता है।
वायरल बुखार की दवा / वायरल बुखार का रामबाण इलाज
वायरल बुखार का इलाज करने के लिए, कुछ उपचार विकल्पों को नीचे समझाने का प्रयास किया गया है:
1. पर्याप्त मात्रा में आराम लेना और पानी पीना: पर्याप्त मात्रा में आराम लेना और पानी पीना, वायरल बुखार का रामबाण इलाज है।
2. बुखार कम करने वाली दवाइयाँ: बुखार कम करने वाली ओवर-द-काउंटर दवाइयों जैसे पेरासिटामोल का उपयोग भी, वायरल बुखार की दवा के रूप में किया जा सकता है।
3. पेन मैनेजमेंट: दर्द निवारक दवाइयों या पेन-किलर्स का उपयोग भी वायरल बुखार का इलाज करने के लिए किया जा सकता है।
4. सिम्प्टोमैटिक रिलीफ: खाँसी और कंजेशन जैसे विशिष्ट लक्षणों को उचित दवाइयों द्वारा ठीक करके, रोगी संपूर्ण रूप से आराम प्राप्त कर सकता है।
5. चिकित्सक से संपर्क करना: सर्दी, खाँसी या बुखार जैसे लक्षणों के बने रहने पर तत्काल चिकित्सक से संपर्क करने से, बहुत सी वायरल बीमारियों से बचने में मदद मिल सकती है।
6. एंटीवायरल दवाइयाँ: कुछ केसेस में, वायरल बुखार का रामबाण इलाज, एंटीवायरल दवाइयाँ भी हो सकती हैं।
वायरल बुखार के लिए सर्वाइवल रेट
वायरल बुखार के लिए सर्वाइवल रेट, बुखार पैदा करनेवाले वायरस के प्रकार, व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य स्थिति और अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियों पर निर्भर करती है। वायरल बुखार के लिए सर्वाइवल रेट बहुत अधिक होती है। यदि इस विषय पर चर्चा करें कि वायरल फीवर कितने दिन रहता है, तो यह आमतौर पर तीन से चार दिन तक रह सकता है। इसके अधिकतर मामले हल्के और स्व-सीमित होते हैं। स्व-सीमित बीमारियों का अर्थ है, वह बीमारियाँ जो बिना किसी उपचार के स्वयं ठीक जाती हैं। हालाँकि, यह याद रखना आवश्यक है कि कुछ मामलों में, कुछ वायरस गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के उत्पन्न होने का कारण बन सकते हैं। विशेष रूप से कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग और बुजुर्गों की स्थिति वायरल इन्फेक्शन के कारण अधिक गंभीर हो सकती है। इन गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों में निमोनिया, अंग विफलता (Organ Failure) या अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ शामिल हैं।
निष्कर्ष
जिस प्रकार घनी आबादी वाले देश भारत में वायरल बुखार के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, यह एक महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य चिंता का विषय बनता जा रहा है। वैसे तो वायरल बुखार के अधिकतर मामले हल्के और स्व-सीमित होते हैं, लेकिन इसके कुछ मामलों में व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर हो सकती है। वायरल बुखार के लिए सर्वाइवल रेट, बुखार पैदा करनेवाले वायरस के प्रकार, व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य स्थिति और अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकती है।
वायरल बुखार के सामान्य लक्षणों में बुखार, शरीर में दर्द, सिरदर्द, थकान, खाँसी और गले में खराश जैसे लक्षण शामिल हैं।
अधिकांश मामलों में, पर्याप्त मात्रा में आराम लेना और पानी पीना, वायरल बुखार का रामबाण इलाज हो सकता है। इसके अतिरिक्त अच्छी स्वच्छता रखने से, टीका लगवाने से, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से बचने से और समय-समय पर स्वास्थ्य पेशेवर से संपर्क करने से, वायरल बुखार के जोखिम को कम करने में बहुत हद तक मदद मिल सकती है।
वायरल बुखार के लक्षण और उपाय या वायरल फीवर के लक्षण और उपचार संक्षेप में
वायरल बुखार के लक्षण और उपाय या वायरल फीवर के लक्षण और उपचार के बारे में जानकारी होने से, वायरल बुखार से छुटकारा पाना संभव हो सकता है। यदि वायरल बुखार के लक्षणों की बात करें, तो इसके लक्षणों में बुखार, शरीर में दर्द, थकान, खाँसी, गले में खराश और नाक बहना इत्यादि शामिल हैं। वायरल बुखार का उपचार करने के लिए, बुखार कम करने वाली दवाइयों या एंटीवायरल दवाइयों का उपयोग किया जा सकता है।
यदि आप भी कैंसर के इलाज का खर्च नहीं जुटा पाने के कारण चिंतित हैं, तो क्राउडफंडिंग की मदद अवश्य लें।